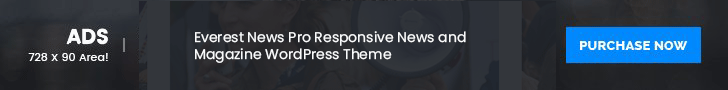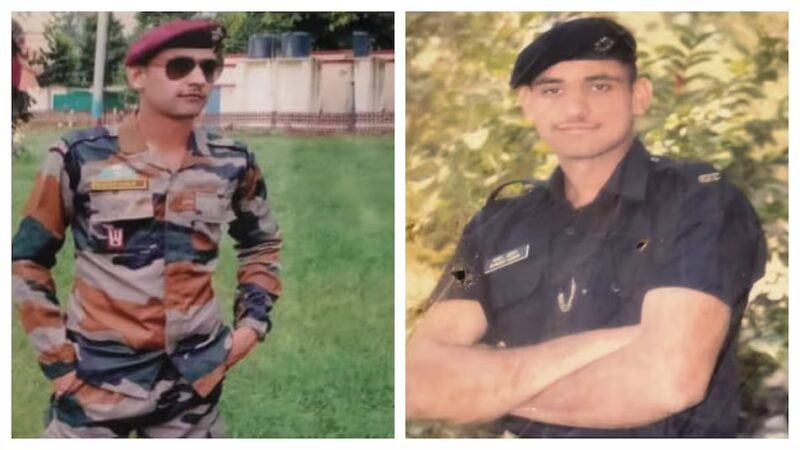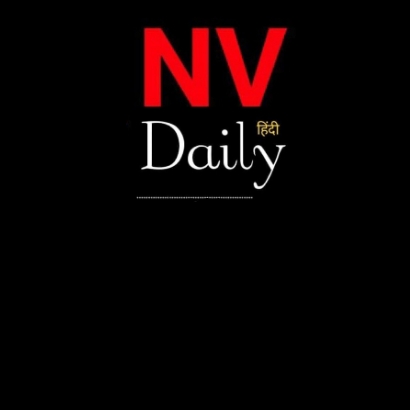स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर स्वास्थ्य पैरेलल हैं, पूरक भी कहे जा सकते हैं। यानी कि एक के बिना दूसरे की कल्पना करना थोड़ी बेमानी सी होगी। हालांकि आधुनिकता, औद्योगिक क्रांति और असीम आवश्यकताओं ने हमारे अस्तित्व के एक पैर को लकवा ग्रस्त कर दिया है। तेजी से विकास की ललक ने हमें इतना आतुर बना दिया है कि आज के चक्कर में स्वयं के ही भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर्यावरण के साथ पिछले कुछ दशकों से जो अत्याचार हो रहा है, वह इसी खिलवाड़ का आईना है। नतीजा, भोजन से लेकर सांस तक, सब जगह बस प्रदूषण और विषाक्तता ही दिख रही है। ऐसी विषाक्तता जो संभवत: अभी नजर न आ रही हो, पर उसके दुष्प्रभाव जरूर देखे जाते रहे हैं।
5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसा खास दिन जब हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर विचार-मंथन करते हैं, लोगों को इसके बारे में सचेत किया जाता है, ताकि हम, हमारी आंखों के सामने ही गड़बड़ा रहे भविष्य को सुधार सकें। पर क्या इस वैश्विक संकट के लिए एक दिन चर्चा कर लेना ही काफी है? क्योंकि पर्यावरण के साथ जो दोहन पिछले कुछ दशकों में हुआ है, उसने दुष्प्रभावों की ऐसी बड़ी खाई बना दी है, जिसे भरना इतना आसान नहीं होने वाला है।
सेहत के नजरिए से देखें तो पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण और रसायनों ने कई तरह से हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि पर्यावरण में बढ़ती विषाक्तता कैंसर जैसे गंभीर रोगों के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा देती है। हवा, पानी, मिट्टी और हमारे भोजन में बढ़ते रसायनों की मात्रा कैंसर का कारण बनने वाले पर्यावरणीय कारकों में से प्रमुख हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के इस लेख में हम हमारे भोजन में बढ़ती विषाक्तता और इसके दुष्प्रभावों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे।
पर्यावरण विषाक्तता और कैंसर का जोखिम
कैंसर के कारकों को लेकर हुए अध्ययन में पाया गया है कि दुनियाभर में हर साल सामने आ रहे कैंसर के मामलों में से 70-90 फीसदी के लिए पर्यावरण और जीवनशैली के कारकों को जिम्मेदार माना जा सकता है। जॉन्स हॉपकिन्स के शोधकर्ताओं का कहना है कि 65% कैंसर के मामले रैंडम डीएनए उत्परिवर्तन का परिणाम हैं, जबकि शेष 35 फीसदी कैंसर के मामलों के लिए पर्यावरणीय और वंशानुगत कारकों के संयोजन को कारक के रूप में देखा जाता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि तंबाकू का धुआं और सूरज की किरणों के कारण होने वाले कैंसर से तो आप बच सकते हैं, पर जिस प्रदूषित हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो प्रदूषित पानी और भोजन हम खा-पी रहे हैं, उससे होने वाले खतरे को कैसे कम किया जा सकेगा?
यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारी थाली में जो भोजन रोजाना आ रहा है, उसमें भी विषाक्तता हो सकती है, इतनी विषाक्तता जो आपको कैंसर का शिकार बना सकती है।
भोजन का विषाक्तता और कैंसर का जोखिम
पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तता की बात करते समय हमेशा ख्याल वायु प्रदूषण की तरफ ही जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि मृदा प्रदूषण भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाने वाला कारक है। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ पर्यावरण और मिट्टी में बढ़ती धातुओं की मात्रा पेट के कैंसर के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा देती है।
इस तरह की मिट्टी में पैदा होने वाले फसलों में भी इस विषाक्तता का अंश शेष रह जाता है जिससे कई तरह की स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। पश्चिमी देशों के आंकड़े उठाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि यहां कैंसर के निदान के 30 फीसदी मामले आहार संबंधी कारकों से जुड़े हुए हैं।
इसे सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम तमाम तरह के रसायनों-उर्वरकों को प्रयोग में लाते हैं। इनमें से कई तो प्रतिबंधित भी हैं। इनके प्रयोग से मिट्टी और फसल दोनों में विषाक्तता बढ़ती है। ऐसे में उस भूमि से होने वाली पैदावार और उन फसलों का सेवन जाने-अनजाने हमें जानलेवा कैंसर के करीब लाता जा रहा है।
विकासशील देशों में और भी खतरा
विकासशील देशों की स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि आहार की विषाक्तता के कारण यहां कैंसर का जोखिम 20 फीसदी के करीब रहता है। उदाहरण के लिए कई शोध में वैज्ञानिकों ने हमारे दैनिक आहार में ऐसे सिंथेटिक्स की मौजूदगी पाई गई है जो सीधे तौर पर लिवर कैंसर का कारण बनती है। फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से नाइट्राइट साल्ट, सोडियम नाइट्राइट (E250), पोटेशियम नाइट्राइट (E249) आदि का प्रयोग किया जाता रहा है। ये न सिर्फ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले होते हैं, साथ ही भोजन में विषाक्तता को बढ़ाकर कई तरह की गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी बढ़ा देते हैं।
प्रतिबंधित रसायनों के छिड़काव से पर्यावरण-भोजन की बढ़ती विषाक्तता
पर्यावरण प्रदूषण और फसलों में रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने न सिर्फ कैंसर, साथ ही कई अन्य रोगों के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जिन अनाजों को स्वस्थ मानकर हम सेवन करते आ रहे हैं, असल में उसकी पैदावार को बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कई ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाता रहा है, जिसे बेहद हानिकारक मानते हुए कई देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने बाकायदा प्रतिबंधित रसायनों की सूची भी साझा की है।
फेडरल इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड एंड रोडेंटिसाइड एक्ट (एफआईएफआरए) संघीय कानून है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कीटनाशकों के पंजीकरण, वितरण, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करता है। इस संस्था ने कई रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग को बैन किया हुआ है, फिर भी कई देशों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी ही कुछ उदाहरण देखिए-
डीडीटी, ऐसा ही एक कीटनाशक है जिसका छिड़काव फसलों को लगने वाले रोग से बचाता है, हालांकि अध्ययनों में इसे अकार्बनिक विषाक्त पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो जल प्रदूषण और पर्यावरण के लिए खतरे का कारण बनता है। फसलों में इसका उपयोग विषाक्तता को बढ़ावा देता है।
नियोनिकोटिनोइड्स और इस वर्ग के कीटनाशकों और रसायनों को यूरोप सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका छिड़काव विभिन्न खाद्य फसलों में अवांछित कीटों को नष्ट करने में सहायक जरूर है, पर इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभावों में पर्यावरण में विषाक्तता बढ़ने और ऐसी फसल के अनाज के सेवन से कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है।
बीएचसी का सामान्य उपयोग बेंजीन हेक्सा क्लोरीन के रूप में किया जाता है। यह एक उद्यान रसायन है जो फसलों को खतरनाक कीटों से सुरक्षा देती है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि रासायनिक स्प्रे के रूप में बीएचसी का उपयोग करने से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। यह इतना नुकसानदायक है कि छिड़काव के बाद अगले 3 से 5 उस मिट्टी की उपज कम हो सकती है। छिड़काव वाले अनाज का सेवन तंत्रिका तंत्र और कोशिकाओं से संबंधित गंभीर रोगों के जोखिम को काफी बढ़ा देता है।
क्या प्लेट में आने वाला भोजन सुरक्षित है?
अब तक के तथ्यों और प्रस्तुत किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट के बाद आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य होगा कि हम रोजाना जिन चीजों का सेवन करते हैं, असल में उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए भी तो हानिकारक और जानलेवा रसायन-कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या यह सुरक्षित है?
यूके कैंसर रिसर्च द्वारा इसी विषय को लेकर किए गए शोध में पाया गया कि फसलों में होने वाले हानिकारक कीटनाशकों और रसायनों के छिड़काव से वैसे तो सीधे तौर पर कैंसर का खतरा नहीं होता है। ऐसी मिट्टी में उपजे फसल में बहुत थोड़ी मात्रा में कीटनाशक हो सकते हैं, इनका स्तर इतना कम होता है कि इसे कैंसर का जोखिम कारक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि अगर प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग और फसलों की रखरखाव के लिए हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग को लेकर सख्ती नहीं बरती गई तो इससे निश्चित ही भविष्य में जोखिम बढ़ सकता है। इस तरह के जोखिमों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोने की सलाह देते हैं।
इस सवाल का दूसरा पहलू भी जरूर आपके लिए विचारणीय है। शोध बताते हैं मांस उत्पादों और सॉसेज में जीवाणुरोधी और केमिकल युक्त रंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रसंस्कृत मांस उत्पादों से आंत के कैंसर का खतरा 21% बढ़ जाता है। इसके अलावा, मूंगफली, दलहन, तिलहन और अनाज में एफ्लाटॉक्सिन पाए गए हैं और ये हेपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के जोखिम को बढ़ाते हैं।
ज्यादा चमकदार और आकर्षक दिखने वाले फलों-सब्जियों से रहें सावधान
बाजार में फलों-सब्जियों को आकर्षक दिखाकर अच्छे दाम पाने का चलन है पर क्या आपने कभी सोचा कि कुछ वर्षों पहले तक भद्दे और छोटे दिखने वाले ये फल अचानक इतने आकर्षक कैसे हो गए? आपको याद है बचपन में तरबूज आज के मुकाबले छोटे, अधिक लाल और मीठे होते थे? सेब चमकदार कम होते थे, आम जून तक पकते थे और केले-भिंडी देखने में अजीब तरह के टेढ़े होते थे, फिर इसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया?
रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पके हुए फलों की शेल्फ लाइफ कम होती है, इसलिए कुछ किसान और आपूर्तिकर्ता उन्हें लंबे समय तक ताजा दिखाने के लिए रसायनों को प्रयोग में लाते हैं, कुछ रसायनों को तो फलों में इंजेक्ट भी कर दिया जाता है। फलों के फसल में दवाइयों का प्रयोग करके उन्हें हाइब्रिड बनाया जा रहा है जिससे वह दिखने में खूबसूरत और आकार में बड़े तो लगते हैं, पर उनमें विषाक्तता अधिक और पोषकता कम होती जा रही है।
इसी तरह मांसाहार का भी हाल है। मांस को चमकदार बनाने के लिए लाल रंगों का इंजेक्शन लगाया जाता हैं। ये रंग जहरीले हो सकते हैं और कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। सेब को भी मोम में लेपित किया जाता है जिससे वह चमकदार दिखने लगें, पर मोम का पेट में जाना समस्याओं को बढ़ा सकता है।
अध्ययनों से पता चलता है कि फलों को आकर्षक बनाने और समय से पहले पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को प्रयोग में लाया जाता है। शोध में पाया गया कि इससे पके फलों के सेवन से हाइपोक्सिया का जोखिम हो सकता है जिसके कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसके कारण सिरदर्द, चक्कर आना, नींद विकार, स्मृति हानि, पैरों और हाथों में सुन्नता और दौरे जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं।
पर्यावरण के नजरिए से बात करें तो अध्ययन में पाया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जल को गंभीर रूप से दूषित कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। एसिटिलीन जिसे एथीन भी कहा जाता है, यह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का सदस्य है। यह अगर पर्यावरण में बढ़ जाए तो तेज घुटन की समस्या हो सकती है। इसके संपर्क में रहने वाले लोगों में चक्कर आने, सिरदर्द, थकान, टेककार्डिया (धड़कन की अनियमितता) मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है। इसकी अधिक मात्रा बेहोशी और गंभीर स्थितियों में मृत्यु के जोखिम को भी बढ़ा सकता है।
पर्यावरण और भोजन की विषाक्तता से बचाव के लिए क्या करें?
उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट हो गया है कि फसलों की उपज, गुणवत्ता, दिखावट को बढ़ाने के लिए जिन रसायनों-कीटनाशकों को प्रयोग में लाया जा रहा है, वह पर्यावरण के साथ हमारी सेहत के लिए भी गंभीर समस्याओं का कारक बनती हैं। अब सवाल है कि आखिर इस जोखिम को कम कैसे किया जाए? इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे पहले वैश्विक स्तर पर रसायनों-कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर बैन लगाने के साथ इसकी देखरेख भी का जानी चाहिए। क्योंकि यह हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के अस्तित्व के लिए खतरा है।
दूसरा किसी भी फल-सब्जी के सेवन से पहले उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें, जिससे उसमें किसी भी प्रकार से विषाक्तता का अंश शेष न रहने पाए। ऐसा करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। दीर्घकालिक उपायों के लिए सरकार-नीति निर्माताओं को व्यापक रूप से ‘थाली की बढ़ती विषाक्तता’ के जोखिम को समझते हुए इससे बचाव के लिए व्यापक रूप से काम करने की आवश्यकता है।
कहीं ऐसे न हो जाए कि आज थोड़ा अधिक पाने की लालच, हमारे भविष्य पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दे। आप भी विचार कीजिएगा।