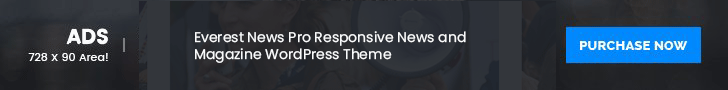— कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्रीय गृहमंत्रालय को दिए तीन महीने
— सभी राज्यों के डीजीपी से कहा- गृहमंत्रालय को भेजें सुझाव
—
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों में पुलिस कर्मियों की मीडिया ब्रीफिंग के बारे में तीन महीने में विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल न्याय के रास्ते से भटका सकता है।
—
नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की तत्काल आवश्यकता है कि पत्रकारों को कैसे जानकारी दी जानी चाहिए क्योंकि 2010 में गृह मंत्रालय द्वारा इस विषय पर पिछली बार दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में आपराधिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग बढ़ी है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मीडिया के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और आरोपी के निष्पक्ष जांच के अधिकार तथा पीड़ित की निजता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए नियमावली तैयार करने के संबंध में एक महीने में गृह मंत्रालय को सुझाव देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, सभी डीजीपी दिशा-निर्देशों के लिए अपने सुझाव एक महीने में गृह मंत्रालय को दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सुझाव भी लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जांच जारी हो तो पुलिस द्वारा “समय से पहले” किया गया। कोई भी खुलासा मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देता है जो न्याय के रास्ते से भटका सकता है क्योंकि यह सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को भी प्रभावित कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसओपी न होने की स्थिति में पुलिस के खुलासे की प्रकृति एक समान नहीं हो सकती क्योंकि यह अपराध की प्रकृति और पीड़ितों, गवाहों व आरोपियों समेत अलग-अलग हितधारकों पर निर्भर करती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी और पीड़ित से जुड़े ऐसे प्रतिस्पर्धी पहलू हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि उनका अत्यधिक महत्व है। शीर्ष अदालत उन मामलों में मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जांच जारी है।
—
न्याय मित्र ने कहा- नहीं रोक सकते रिपोर्टिंग
इस मामले में अदालत की मदद के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि प्रेस को रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सूचना के स्रोत, जो अक्सर सरकारी संस्थाएं होती हैं, को विनियमित किया जा सकता है। उन्होंने 2008 के आरुषि तलवार हत्याकांड का हवाला दिया जिसमें कई पुलिस अधिकारियों ने मीडिया के सामने घटना के संबंध में अलग-अलग बयान दिए थे। 13 वर्षीय आरुषि तलवार और एक बुजुर्ग घरेलू सहायक हेमराज की नोएडा के एक घर में हत्या कर दी गई थी और इस वारदात में आरुषि के माता-पिता पर संदेह किया गया था।
—
जनवरी में अगली सुनवाई
पीठ ने संवेदनशीलता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक महीने के भीतर गृह मंत्रालय को सुझाव सौंपने का निर्देश दिया गया है और अगली सुनवाई जनवरी में होगी।
—
सभी राज्यों के डीजीपी को निर्देश
पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए नियमावली तैयार करने के संबंध में एक महीने में गृह मंत्रालय को सुझाव देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा, सभी डीजीपी दिशा-निर्देशों के लिए अपने सुझाव एक महीने में गृह मंत्रालय को दें…एनएचआरसी के सुझाव भी लिए जा सकते हैं।
–
हमें ‘मीडिया ट्रायल’ की अनुमति नहीं देनी चाहिए
कोर्ट ने तर्क दिया, बुनियादी स्तर पर भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर मीडिया के विचारों और समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार के संदर्भ में शामिल है, लेकिन हमें ‘मीडिया ट्रायल’ की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लोगों को यह अधिकार है कि वे जानकारी तक पहुंचें। लेकिन, अगर जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत सामने आते हैं, तो जांच प्रभावित भी हो सकती है।
–
आरोपी निर्दोष होने का अनुमान लगाने का हकदार
कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस आरोपी के आचरण की जांच चल रही है, वह निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच का हकदार है। हर स्तर पर, हर आरोपी निर्दोष होने का अनुमान लगाने का हकदार है। किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। मार्च में, मुख्य न्यायाधीश ने पत्रकारों से \”रिपोर्टिंग में सटीकता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के मानकों को बनाए रखने\” का आग्रह किया था और कहा था, भाषणों और निर्णयों का चयनात्मक उद्धरण चिंता का विषय बन गया है। इस प्रथा में जनता के विचारों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है। न्यायाधीशों के निर्णय अक्सर जटिल और सूक्ष्म होते हैं, और चयनात्मक उद्धरण यह आभास दे सकते हैं कि निर्णय का अर्थ न्यायाधीश के इरादे से कुछ अलग है।
0000